प्रेम सिंह
एक बार फिर नवउदारवाद
पिछली बार की तरह इस बार भी राष्ट्रपति
चुनाव लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। राष्ट्र के सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख के
चुनाव के अवसर पर चर्चा होना अच्छी बात है। इस अवसर पर चर्चा के कई बिंदु हो सकते
है। मसलन,
चर्चा में पिछले राष्ट्रपतियों के चुनाव, समझदारी
और विशेष कार्यों का आलोचनात्मक स्मरण किया जाए। यहां हम याद दिलाना चाहेंगे कि
देष के दो बार राष्ट्रपति रहे डॉ. राजेंद्र प्रसाद की डॉ. लोहिया ने इस बात के लिए
कड़ी आलोचना की थी कि उन्होंने राष्ट्रपति रहते बनारस के पंडितों के पैर पखारे थे।
संविधान निर्माण के समय की राष्ट्रपति संबंधी बहसों का स्मरण भी किया जा सकता है।
संसदीय प्रणाली की जगह राष्ट्रपति प्रणाली लागू करने की जो बात अक्सर होती है -
अक्सर यह मान कर कि अमेरिका की तरह भारत में भी राष्ट्रपति प्रणाली अपना ली जाए तो
सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी - उस पर गंभीर बहस चलाई जाए। कहने की जरूरत नहीं कि
संविधान का अभिरक्षक (कस्टोडियन) होने के नाते राष्ट्रपति के व्यक्तित्व, पद
और भूमिका को लेकर पूरी चर्चा भारत के संविधान की संगति में हो, न
कि उससे स्वतंत्र। इस तरह राष्ट्रपति चुनाव का अवसर हमारे संवैधानिक नागरिक बोध को
पुष्ट करने में सहायक हो सकता है।
लेकिन जो चर्चा चल रही है उससे लगता है कि
हमारे लिए राष्ट्रपति चुनाव कोई महत्व का अवसर नहीं है। मीडिया और राजनीतिक
पार्टियां दोनों का संदेष यही है कि महत्व की बात केवल यह है कि कौन राजनीतिक
पार्टी या नेता अपना आदमी राष्ट्रपति बना कर राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करता है।
(आगे देखेंगे कि यह जरूरी नहीं कि राजनीति से बाहर का सर्वसम्मति से चुना गया
व्यक्ति राजनेता के मुकाबले संविधान की कसौटी और अन्य अपेक्षाओं पर ज्यादा खरा
उतरता हो।) इस बार के चुनाव में राजनीतिक पार्टियां और नेता दांव-पेच में कुछ
ज्यादा ही उलझे हैं। किसी ने गुगली फेंकी है तो कोई पांसा फेंक रहा है!
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को राष्ट्रपति बनाने का सुझाव फेंका गया तो यह पूरा
प्रकरण एक एब्सर्ड ड्रामा जैसा लगने लगा। जो दांव-पेच हुए और आगे होने की संभावना
है,
उनका पूरा ब्यौरा देने लगें तो कॉलम उसी में सर्फ हो जाएगा।
एक वाक्य में कहें तो यह पूरा प्रकरण भारतीय राजनीति की दिषाहीनता दर्षाता है। कई
बार दिषाहीनता का संकट सही दिषा के संधान में सहायक हो सकता है। बषर्ते उसके पीछे
एक वाजिब दिषा की तलाष की प्रेरणा निहित हो। लेकिन मुख्यधारा भारतीय राजनीति की
दिषाहीनता की एक ही दिषा है - नवउदारवाद की तरफ अंधी दौड़। राष्ट्रपति का चुनाव उसी
अंधी दौड़ की भेंट चढ़ चुका है। राष्ट्रपति संविधान का अभिरक्षक कहलाता है, लेकिन
पूरी चर्चा में - चाहे वह विद्वानों की ओर से हो, नेताओं
या उम्मीदवारों की ओर से - वह नवउदारवाद के अभिरक्षक के रूप में सामने आ रहा है।
किसी कोने से यह चर्चा नहीं आई है कि राष्ट्रपति को पिछले 25
सालों में ज्यादातर अध्यादेषों के जरिए नवउदारवाद के हक में बदल डाले गए संविधान
की खबरदारी और निष्ठा के साथ निगरानी करनी है; कि
ऐसा राष्ट्रपति होना चाहिए जो संविधान को पहुंचाई गई चौतरफा क्षति को समझ कर उसे
दुरुस्त करने की प्रेरणा से परिचालित हो; और
जो संविधान के समाजवादी लक्ष्य से बंधा हो।
जाहिर है, नवउदारवाद
को अपना चुकी कांग्रेस और भाजपा की तरफ से ऐसा उम्मीदवार नहीं आएगा। क्षेत्रीय
पार्टियां भी कांग्रेस-भाजपा के साथ नवउदारवादी नीतियों पर चलती हैं। उनमें कई
अपने को समाजवादी भी कहती हैं। उनमें एक जनता दल (यू) है जिसके प्रवक्ता ने
कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव मुखर्जी के समर्थन में कहा है कि नवउदारवादी आर्थिक
नीतियां अटल हैं। उनके मुताबिक भाजपा के प्रवक्ता रवि प्रसाद वित्तमंत्री बन जाएं
तो वे भी वही करेंगे जो प्रणव मुखर्जी ने किया है। सीधे समाजवादी नाम वाली
समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह की भूमिका को देख कर लगता नहीं कि जिस
लोहिया को वे मायावती के अंबेडकर की काट में इस्तेमाल करते हैं, उस
महान समाजवादी चिंतक की एक पंक्ति भी उन्होंने पढ़ी है। बीजू जनता दल और अन्ना
द्रमुक पीए संगमा की उम्मीदवारी के प्राथमिक प्रस्तावक हैं। संगमा ने प्रणव
मुखर्जी को बहस की चुनौती दी है। इसलिए नहीं कि बतौर वित्तमंत्री उन्होंने
नवउदारवादी आर्थिक नीतियों को लागू करके संविधान विरोधी कार्य किया है। बल्कि
नवउदारवादी आर्थिक नीतियां तेजी से लागू करने में उनकी विफलता उद्घाटित करने के
लिए वे प्रणव मुखर्जी से षास्त्रार्थ करना चाहते हैं। वे अपने को नवउदारवादी
नीतियों का प्रणव मुखर्जी से बड़ा विषेषज्ञ और समर्थक मानते हैं।
प्रणव मुखर्जी के समर्थन पर जिस तरह से
राजग में विभाजन हुआ है, उसी तरह वाम मोर्चा
भी विभाजित है। हालांकि वाम मोर्चा का विभाजन ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि
वह समाजवाद के लक्ष्य से परिचालित एक विचारधारात्मक मोर्चा है जो पिछले करीब चार
दषकों से कायम चला आ रहा है। वाम मोर्चा में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने
प्रणव मुखर्जी का समर्थन किया है जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का मतदान में
हिस्सा नहीं लेने का फैसला है। माकपा के साथ फारवर्ड ब्लॉक है और सीपीआई के साथ
आरएसपी। माकपा ने पिछली बार भी प्रतिभा पाटिल की जगह प्रणव मुखर्जी का नाम
कांग्रेस अध्यक्ष के सामने रखा था। तब वाम मोर्चा की ताकत ज्यादा थी और पष्चिम
बंगाल में माकपा नीत वाम मोर्चा की सरकार थी।
समर्थन का माकपा का तर्क अजीब और खुद की
पार्टी की लाइन के विपरीत है। जैसा कि प्रकाष करात ने कहा है, राष्ट्रपति
का चुनाव विचारधारा के बाहर कैसे हो गया? अगर
मार्क्सवादी विचारधारा के बाहर मान भी लें, तो
क्या वह संविधान की विचारधारा के भी बाहर माना जाएगा? राष्ट्रपति
संविधान का अभिरक्षक होता है, फिर इसके क्या मायने
रह जाते हैं? भारत में मार्क्सवादी विमर्ष और पार्टी
अथवा संगठन तंत्र की अपनी दुनिया है। उसका अपना षास्त्र एवं षब्दावली और उसके आधार
पर आपसी सहयोग और टकराहटें हैं। माकपा के इस फैसले पर कम्युनिस्ट सर्किल में बहस
चल रही है और उसे सही नहीं माना जा रहा है। खुद माकपा के षोध प्रकोष्ठ के एक युवा
नेता ने फैसले को सिरे से गलत और पार्टी लाइन के विपरीत बताते हुए अपने पद से
इस्तीफा दिया है। माकपा ने उसे पार्टी से ही बाहर कर दिया है। माकपा का कहना है कि प्रणव मुखर्जी की
व्यापक स्वीकृति है और माकपा की ताकत विरोध करने की नहीं है। सवाल है कि क्या
व्यापक स्वीकृति नवउदारवाद की नहीं है? तो
क्या उसका विरोध न करके उसके साथ हो जाना चाहिए? स्पष्ट
है कि माकपा का फैसला पष्चिम बंगाल की राजनीति से संबद्ध है। अपनी प्रतिद्वंद्वी
ममता बनर्जी द्वारा प्रणव मुखर्जी के विरोध के चलते माकपा ‘बंगाली
मानुष’
को रिझाने के लिए मुखर्जी का समर्थन कर रही है।
लेकिन इसमें विचारधारात्मक उलझन भी षामिल
है। संकट में घिरी माकपा भारतीय समाजवाद की बात करने के बावजूद पूंजीवाद के बगैर
समाजवाद की परिकल्पपना नहीं सोच पाती है। उसके सामने दो ही रास्ते हैं - या तो वह
पूंजीवाद का मोह छोड़े या एकबारगी पूंजीवाद के पक्ष में खुल कर मैदान में आए। एक
दूसरी उलझन भी है। मार्क्सवादियों के लिए भारत का संविधान (और उसके तहत चलने वाला
संसदीय लोकतंत्र) समाजवादी क्रांति में बाधा है। उन्होंने मजबूरी में उसे स्वीकार
किया हुआ है। इसलिए संविधान के प्रति सच्ची प्रेरणा उनकी नहीं बन पाती। तीसरी उलझन
यह है कि आज भी वे राजनीति की ताकत के पहले पार्टी की ताकत पर भरोसा करते हैं।
संगठन से बाहर - चाहे वह पार्टी का हो, लेखकों
का,
या सरकार का - मार्क्सवादी असहज और असुरक्षित महसूस करते
हैं। लिहाजा, बाहर की दुनिया उनके लिए ज्यादातर सिद्धांत
बन कर रह जाती है। इसके चलते राजनीतिक ताकत का विस्तार नहीं हो पाता।
अच्छा यह होता कि वाम मोर्चा अपना
उम्मीदवार खड़ा करता। चुनावी गणित में वह कमजोर होता, लेकिन
जब तक जनता तक यह संदेष नहीं जाएगा कि उसकी पक्षधर राजनीति कमजोर है, तब
तक वह उसे ताकत कैसे देगी? अभी तो यह हो रहा है
कि खुद जनता की पक्षधर राजनीति के दावेदार यह कह कर मुख्यधारा के साथ हो जा रहे
हैं कि उनकी चुनाव लड़ने की ताकत नहीं है। अकेली आवाज, अगर
सच्ची है,
तो उसे अपना दावा पेष करना चाहिए। नवउदारवादी साम्राज्यवाद
के इस दौर में समाजवादी राजनैतिक चेतना के निर्माण का यही एक रास्ता है जो संविधान
ने दिखाया है। जरूरी नहीं है कि नवउदारवाद की पैरोकार राजनीतिक पार्टियों के सभी
नेता और कार्यकर्ता नवउदारवाद के समर्थक हों। वे भी उठ खड़े हो सकते हैं और अपनी पार्टियों
में बहस चला सकते हैं। कहने का आषय यह है कि नवउदारवाद समर्थक प्रणव मुखर्जी और
पीए संगमा के मुकाबले में वाम मोचा्र की तरफ से एक संविधान समर्थक उम्मीदवार दिया
जाना चाहिए था।
वह उम्मीदवार राजनीतिक पार्टियों के बाहर
से भी हो सकता था। जैसे कि जस्टिस राजेंद्र सच्चर का नाम सामने आया था। लेकिन उस
दिषा मेंं आगे कुछ नहीं हो पाया। जबकि नागरिक समाज संविधान के प्रति निष्ठावान
किसी एक व्यक्ति को चुन कर नवउदारवादी हमले के खिलाफ एक अच्छी बहस इस बहाने चला
सकता था। ऐसे व्यक्ति का नामांकन नहीं भी होता, तब
भी उद्देष्य पूरा हो जाता। लेकिन भारत के नागरिक समाज की समस्या वही है जो
मुख्यधारा राजनीति में बनी हुई है। वहां समाजवादी आस्था वाले लोग बहुत कम हैं।
ज्यादातर आर्थिक सुधारों की तेज रफ्तार के सवार हैं। यही कारण है कि जस्टिस सच्चर
अथवा किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में नागरिक समाज की ओर से मजबूत प्रयास नहीं हो
पाया।
कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का यह चुनाव
संकट के समाधान की दिषा में कोई रोषनी नहीं दिखाता। बल्कि संकट को और गहरा करता
है। प्रणव मुखर्जी की राष्ट्रपति के रूप में जीत को मनमोहन सिंह और मंटोक सिंह
आहलुवालिया आर्थिक सुधारों को तेज करने का अवसर बनाएंगे। प्रणव मुखर्जी के
राष्ट्रपति चुनाव जीतते ही सबसे पहले संभवत: खुदरा क्षेत्र में 51
प्रतिषत विदेषी निवेष के स्थगित फैसले को लागू कर दिया जाएगा।
यह भी कह सकते हैं कि इस संकट से जूझा जा
सकता था,
बषर्ते नागरिक समाज संविधान की टेक पर टिका होता। हम
नक्सलवादियों को बुरा बताते हैं और उन पर देषद्रोह का अपराध जड़ते हैं, क्योंकि
वे भारत के संविधान को स्वीकार नहीं करते। लेकिन नक्सलवादियों को देषद्रोही बताने
वाले राजनेताओं और नागरिक समाज एक्टिविस्टों की संविधान के प्रति अपनी निष्ठा
सच्ची नहीं हैं। पिछले 25 सालों में यह
उत्तरोत्तर सिद्ध होता गया है। इस चुनाव से भी यही सबक मिलता है।
टीम अन्ना ने प्रधानमंत्री समेत उनकी
केबिनेट के जिन मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं उनमें प्रणव मुखर्जी भी
हैं। वे राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। यह स्पष्ट हो चुका है कि टीम अन्ना की लड़ाई
भ्रष्टाचार से उतनी नहीं, जितनी कांग्रेस से
ठन गई है। प्रणव मुखर्जी का राष्ट्रपति बनना कांग्रेस की जीत है। भाजपा कांग्रेसी
उम्मीदवार को रोकने की, या कम से कम उसे
मजबूत टक्कर देने की रणनीति नहीं बना पाई। उसके वरिष्ठतम नेता अडवाणी दयनीयता से
कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के नाम पर सर्वसम्मति बनाने के लिए
भाजपा से बात नहीं की। ममता बनर्जी अभी यूपीए से निकली नहीं हैं और मुलायम सिंह
झोली में गिरने को तैयार बैठे हैं। भाई रामगोपाल यादव को उपराष्ट्रपति का पद मिल
जाए,
दूसरे भाई षिवपाल यादव और बहू डिंपल केंद्र में मंत्री बन
जाएं तो परिवार के मुखिया का कर्तव्य संपूर्ण हो जाएगा! आरएसएस हालांकि मोदी पर
अड़ेगा नहीं, लेकिन ‘विनाष
काले विपरीत बुद्धि’ हो जाए तो राजग के
घटक दल ही नहीं, भाजपा में भी विग्रह तेज होगा। ऐसी स्थिति
में 2014
में कांग्रेस की पक्की हार मानने वाले टीम अन्ना के कुछ सदस्य अभी से अलग लाइन पकड़
सकते हैं। वैसे भी राजनीति से दूर रहने की बात केवल कहने की है। केजरीवाल और
प्रषांत भूषण चुनाव लड़ने की संभावनाएं तलाषते घूम रहे हैं। रामदेव गडकरी से लेकर
बर्द्धन तक न्ेता-मिलाप करते घूम रहे हैं। ये सब एक ही टीम है - नवउदारवाद की
पक्षधर और पोषक। इनके पास सारा धन इसी भ्रष्ट व्यवस्था से आता है। अपने नाम और
नामे के फ्रिक्रमंद ये सिविल सोसायटी एक्टिविस्ट भला किसी सही व्यक्ति के नाम पर
अड़ कर अपनी ऊर्जा क्यों बरबाद करते?
बहरहाल, कई
नाम चर्चा में आने के बाद दो उम्मीदवार तय हो गए हैं। यूपीए की तरफ से प्रणब
मुखर्जी और एनडीए की तरफ से पीए संगमा। कांग्रेस में राष्ट्रपति पद के लिए
कांग्रेस प्रत्याषी का चुनाव सोनिया गांधी ने किया। पार्टी के नेताओं ने इसके लिए
बाकायदा उनसे गुहार लगाई। जैसे संसद में सब कुछ तय करने का अधिकार सोनिया गांधी का
है और विधानसभा में एमएलए प्रत्याशी से लेकर मुख्यमंत्री तक तय करने का अधिकार है, उसी
तरह राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार भी वे स्वयं ही तय करती हैं। पिछली बार भी
उन्होंने यही किया था। इससे कांग्रेस पर तो क्या फर्क पड़ना है, राष्ट्रपति
पद की गरिमा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
जैसा कि कहा जा रहा है, प्रणव
मुखर्जी बहुत हद तक सर्वस्वीकार्य हैं। लेकिन सोनिया गांधी ने उस वजह से उन्हें
उम्मीदवार नहीं बनाया है। सोनिया गांधी के प्रति व्यक्तिगत और नवउदारवाद के प्रति
विचारधारागत समर्पण की लंबी तपस्या के बाद उन्हें रायसीना हिल पर आराम फरमाने का
पुरस्कार दिया गया है। हालांकि तपस्यारत प्रणव मुखर्जी को, कहते
हैं,
प्रधानमंत्री पद की आषा थी। लेकिन सोनिया गांधी किसी
राजनीतिक व्यक्ति को इस पद के आस-पास नहीं फटकने दे सकतीं। नवउदारवादी प्रतिष्ठान
सोनिया गांधी को स्वाभाविक तौर पर अपना मानता है। सोनिया गांधी की ताकत का स्रोत
केवल कांग्रेसियों द्वारा की जाने वाली उनकी भक्ति नहीं है। केवल उतना होता तो अब
तक तंबू गिर चुका होता। वैष्विक पूंजीवादी ताकतें उन्हें सत्ता के षीर्ष पर बनाए
हुए हैं।
जाहिर है, सर्वस्वीकार्य, अनुभवी
और योग्यतम प्रणव मुखर्जी किसी गंभीर दायित्व-बोध के तहत राष्ट्रपति के चुनाव में
नहीं हैं। बल्कि यह चुनाव उनका अपना है ही नहीं। वे चुनाव जीतेंगे और संविधान की
एक बार फिर हार होगी। पार्टी और सरकार से विदाई के बिल्कुल पहले तक आर्थिक सुधारों
की रफ्तार तेज करने की जरूरत बताने वाले प्रणव मुखर्जी की डोर राष्ट्रपति भवन में
भी सुधारों के साथ बंधी रहेगी।
दूसरे उम्मीदवार संगमा भी किसी गंभीर
दायित्व-बोध के तहत चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। बल्कि अपने अब तक के राजनैतिक कैरियर
का उत्कर्ष हासिल करने के लिए मैदान में हैं। वे सत्ता के सुख में मगन रहने वाले
नेता हैं जो 1977 से अब तक आठ बार लोकसभा के सदस्य चुने गए
हैं। वे केंद्र में मंत्री रहे हैं, मेघालय
के मुख्यमंत्री रहे हैं और सर्वसम्मति से लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। उनकी
बेटी केंद्र में मंत्री है और बेटा मेघालय में। कांग्रेस से राकांपा, राकांपा
से तृणमूल कांग्रेस, फिर राकांपा और अपनी
उम्मीदवारी न छोड़ने के चलते अब राकांपा से बाहर हैं। इस पद पर उनकी पहले से नजर
थी। कोई आदिवासी अभी तक राष्ट्रपति नहीं बना है, यह
तर्क उन्होंने अपने पक्ष में निकाला और पांच-छह लोगों का ट्राइबल फॉरम ऑफ इंडिया
बना कर खुद को उस फॉरम का उम्मीदवार घोषित कर दिया। यह कहते हुए कि वे देष के
करोड़ों आदिवासियों के प्रतिनिधि हैं।
संयोग से हमें एक टीवी चैनल पर संगमा का
इंटरव्यू सुनने को मिल गया। तब तक भाजपा ने उन्हें अपना उम्मीदवार स्वीकार नहीं
किया था। इंटरव्यू के अंत का भाग ही हम सुन पाए। उनके जवाब कहीं से भी राष्ट्रपति
के पद की गरिमा के अनुरूप नहीं थे। जिस सर्वोच्च पद के लिए वे खड़े हैं, अपने
को उसके के लिए उन्होंने कतई तैयार नहीं किया है। वे राजनीति का मतलब अपने और अपने
बच्चों के लिए बड़े-बड़े पदों की प्राप्ति मानते हैं। यह सब उन्हें मिला है, इसके
लिए उन्होंने ईष्वर को धन्यवाद दिया। लेकिन राजनीतिक सत्ता की उनकी भूख किंचित भी
कम नहीं हुई है। वे अपनी और अपने बच्चों की और बढ़ती देखना चाहते हैं। जब एंकर ने
पूछा कि अभी तो वे काफी स्वस्थ हैं और आगे की बढ़ती देख पाएंगे तो उन्होंने कहा कि
राजेश पायलट कहां देख पाए अपने बेटे को मंत्री बने? यानी
जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कब दगा दे जाए, इसलिए
जो पाना है जल्दी से जल्दी पाना चाहिए। उन्होंने अंत में यह संकेत भी छोड़ा कि इस
बार न सही, अगली बार उन्हें राष्ट्रपति बनाया जाए।
उपनिवेषवादी दौर रहा हो, आजादी
के बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था का दौर रहा हो या पिछला 25
सालों का नवउदारवादी दौर - विकास के पूंजीवादी मॉडल की सबसे ज्यादा तबाही
आदिवासियों ने झेली है। संगमा उत्तर-पूर्व से हैं। वहां के आदिवासियों और षेष भारत
के आदिवासियों की स्थितियों में ऐतिहासिक, भौगोलिक
व सांस्कृतिक कारकों के चलते फर्क रहा है। पूंजीवाद का कहर बाकी भारत के
आदिवासियों पर ज्यादा टूटा है। संगमा आदिवासियों की तबाही करने वाली राजनीति और
विकास के 1977 से अग्रणी नेता रहे हैं। उन्होंने कभी
आदिवासियों के लिए आवाज नहीं उठाई। आदिवासियों को उजाड़ने वाली राजनीति के सफल नेता
रहे संगमा अब उनके नाम पर राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। सत्ता की उनकी भूख इतनी ‘सहज’ है
कि वे किसी भी समझौते के तहत मैदान से हट कर उपराष्ट्रपति बनने को तैयार हो सकते
हैं। ताकि आगे चल कर राष्ट्रपति बन सकें।
हवाई सपनों के सौदागर डॉ. कलाम
पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का नाम
भी देर तक चलता रहा। ममता बनर्जी ने उन्हें उम्मीदवार बनाना चाहा और भाजपा ने।
मुलायम सिंह ने जो तीन नाम उछाले थे उनमें डॉ. कलाम का नाम भी था। जिस तरह पिछली
बार डॉ. कलाम ने दूसरा कार्यकाल पाने के लिए कोषिष की थी, इस
बार भी सक्रिय नजर आए। पिछली बार की तरह इस बार भी फेसबुक पर उनके लिए लॉबिंग की
गई। उन्हें षायद आषा रही होगी कि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की दाब में कांगेस
उन्हें समर्थन दे देगी और वे एक बार फिर सर्वसम्मत उम्मीदवार बन जाएंगे। लेकिन
प्रणव मुखर्जी का नाम तय होने और उन्हें व्यापक समर्थन मिलने के बाद जब देखा कि
जीत नहीं फजीहत होने वाली है, अपनी उम्मीदवारी से
इनकार कर दिया।
याद करें प्रतिभा पाटिल के राष्ट्रपति बनने
पर काफी नाक-भौं सिकोड़ी गई थी। इसलिए नहीं कि वे बतौर राष्ट्रपति अपेक्षाएं पूरा
नहीं कर सकती थीं, या उन्होंने चुनाव
के पहले ही अपने दिवंगत गुरु से वार्तालाप संबंधी ‘रहस्य’ का
उद्घाटन कर दिया था। या इसलिए कि सोनिया गांधी ने उन्हें थोप दिया था। बल्कि
इसलिए कि उनका अपीयरेंस एक ग्रामीण महिला जैसा है; वे
विदेष में भारत की बेइज्जती कराएंगी। हमने यह खास तौर गौर किया था कि मध्य वर्ग से
आने वाले हमारे छात्र, जिनके अपने
माता-पिता प्रतिभा पाटिल जैसे लगते होंगे, देश
की बेइज्जती कराने का तर्क ज्यादा दे रहे थे। उनमें भी खास कर लड़कियां। उन्हें यह
भी शिकायत थी कि प्रतिभा पाटिल फर्राटे से अंग्रेजी नहीं बोलती। उन्हें डॉ. कलाम
जैसा हाईफाई राष्ट्रपति चाहिए था।
प्रतिभा पाटिल अपना कार्यकाल ठीक-ठाक निभा
ले गईं। उन्होंने कुछ भी खास नहीं किया। संविधान पर जो कुठाराघात हो रहा है, उस
तरफ उन्होंने इशारा तक नहीं किया। स्त्री सशक्तिकरण का तर्क सोनिया गांधी ने दिया
था। उस दिषा में उन्होंने कुछ भी विषेष नहीं किया। लेकिन यह स्वीकार करना होगा कि
उन्होंने डॉ. कलाम जैसी हवाई बातें कभी नहीं कीं। हम इसे उनका एक बड़ा गुण मानते
हैं। अपनी छवि चमकाने के लिए जिस तरह से डॉ. कलाम ने राष्ट्रपति के ओहदे से हवाई
बातें की,
वह गलत परंपरा थी जिसे प्रतिभा पाटिल ने तोड़ा। डॉ. कलाम की
हाई-हवाई बातों में युवा ही नहीं, कई वरिष्ठ लोग भी आ
गए थे। उसीका सरमाया खाने के लिए वे दो बार फिर से राष्ट्रपति बनने के लिए उद्यत
दिखे। उनकी अवकाश-प्राप्ती के अवसर पर हमने ‘युवा
संवाद’
(अगस्त 2007) में ‘हवाई
सपनों के सौदागर डॉ. कलाम’ षीर्षक से लेख लिखा
था जो इस प्रकार है :
‘‘जिन कलाम साहब के बारे में यह कहा गया कि
उन्होंने अपने कार्यकाल में ‘प्रेसीडेंसी’ के
मायने बदल दिए, मैं कभी उनका प्रषंसक नहीं हो सका। मैंने
काफी कोषिष की उनकी सराहना कर सकूं, लेकिन
वैसा नहीं हुआ। यह मेरी सीमा हो सकती है और उस सीमा के कई कारण। मुझे उनके विचारों
में न कभी मौलिक चिंतन की कौंध प्रतीत हुई, न
इस देष की विषाल वंचित आबादी के प्रति करुणा का संस्पर्ष। जिस तरह की हाई-हवाई
बातें वे करते रहे और उनके गुणग्राहक उनका बढ़ा-चढ़ा कर प्रचार करते रहे, उसके
बाद यह सोचना मुष्किल है कि अपनी ऊंची उड़ान में कलाम साहब कभी इस ‘अपराधबोध’ का
षिकार होते हों कि ‘आदर्षवादियों’ ने, मुक्तिबोध
के षब्दों में, देष को मार कर अपने आप को जिंदा रखा है।
राष्ट्राध्यक्षों का प्रेरणादायी भाषण देना, सपने
दिखाना आम रिवाज है। लेकिन निराधार प्रेरणा और सपने का कोई अर्थ नहीं होता। उनके
नीचे ठोस जमीन होनी चाहिए।
यह लेख मैं नहीं लिखता अगर सुरेंद्र मोहन
और कुलदीप नैयर जैसे समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा में विष्वास रखने
वाले दो वरिष्ठतम विद्वान अवकाष ग्रहण करने के अवसर पर राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल
कलाम की अतिरंजनापूर्ण बड़ाई नहीं करते। सुरेंद्र मोहन जी तो अपनी प्रषंसात्मक
अभिव्यक्ति को ‘न भूतो, न
भविष्यति’
तक खींच लाए। वे लिखते हैं : ‘सपनों
को जगाने वाला, आषाओं और उमंगों को हर दिल में बसाने वाला
और नई दृष्टियों का संवाहक डॉ. अब्दुल कलाम जैसा राष्ट्रपति फिर कभी भारत को मिल
पाएगा यह कहना कठिन ही है। राष्ट्र को ऐसा विज्ञानवेत्ता और यांत्रिकी का विषेषज्ञ
राष्ट्रपति अब तक नहीं मिला था। न वे भाषणकला के धनी थे और न ही डॉ. राजेंद्र
प्रसाद या वेंकटरमण की तरह संविधानवेत्ता ही थे। डॉ. जाकिर हुसैन और डॉ. षंकरदयाल
षर्मा राजनीतिक, प्रषासन और षिक्षा के क्षेत्रों के
सम्मानित विद्वान थे, इन गुणों से भी डॉ.
कलाम का संबंध नहीं था। इसके बावजूद जो अपार लोकप्रियता, खास
कर नई नस्लों का असीम प्यार डॉ. कलाम को मिला, वह
षायद अन्य किसी पूर्व राष्ट्रपति को नहीं मिला। सपनों, कल्पनाओं, उमंगों
और अरमानों से सभी दिलों को भरने वाला ऐसा प्रेरणादायक षिक्षक न तो कभी इस
गौरवपूर्ण पद पर बैठा है है, न बैठेगा - न भूतो, न
भविष्यति।’ (‘दैनिक भास्कर’, 22
जुलाई 2007)
इस तरह सुरेंद्र जी ने ‘सपनों
के सौदागर’ कलाम साहब को षाीषे में उतार दिया है, जो ‘अर्थषास्त्रियों
से कहते रहे हैं कि मनुष्य सिर्फ पेट की भूख से ही नहीं तड़पता, उसे
ज्ञान का प्रकाष भी चाहिए।’ (वही) यह अफसोस की
बात है कि सुरेंद्र जी की पैनी नजर सतह पर तैरती यह सच्चाई नहीं देख पाती कि कलाम
साहब जैसों की दुनिया में ज्ञान का प्रकाष पाए लोगों का पेट कभी नहीं भरता। कलाम
साहब के कार्यकाल में उन्हीं के हस्ताक्षर से स्वीकृत हुआ सांसदों और विधायकों के
लाभ के पद से संबंधित विधेयक इसका एक छोटा-सा उदाहरण है। यह कहना कि कलाम साहब खुद
सादगी पसंद हैं, कोई मायने नहीं रखता। जिस देष में सरकार के
अनुसार देष की आधी से ज्यादा आबादी - नौनिहालों, नौजवानों, महिलाओं, बुजुर्गों
समेत - हर तरह और हर तरफ से असुक्षिरत है, वहां
कलाम साहब और मनमोहन सिंह जैसों की सादगी ‘षाही’ कही
जाएगी। उस तंत्र का हिस्सा होना जो ऐष्वर्य और ऐषोआराम में मध्यकालीन षासकों को
लज्जित करने वाला है, सादगी के अर्थ को
षून्य कर देता है।
उपर्युक्त कथन के पूर्व सुरेंद्र जी ने
लिखा है : ‘डॉ. कलाम देष को उस अंधी दौड़ से ऊपर उठाना
चाहते हैं, जो हमें अमेरिका की राह पर ले जाती है, जहां
अमीरी और गरीबी में बहुत अंतर है और एक सैंकड़ा लोग देष के पचीस सैंकड़ा गरीबों की
समूची संपत्ति से भी अधिक संपत्ति के स्वामी हैं।’ हमें
याद नहीं पड़ता कि कलाम साहब ने देष की अर्थनीति से लेकर राजनीति तक को अमरीकी पटरी
पर डालने वाली मौजूदा या पिछली सरकार को कभी इसके प्रति आगाह किया हो। हमें यह भी
नहीं लगता कि देष के अमरीकीकरण का विरोध करने वाले आंदोलनों और उनके
नेताओं-विचारकों के बारे में कलाम साहब को कोई जानकारी या सहानुभूति हो। वे देष
में दो राजनीतिक पार्टियां होने के समर्थक हैं। वे दो पार्टियां कांग्रेस और भाजपा
ही हो सकती हैंं। ये दोनों देष को अमरीका के रास्ते पर चलाने वाली हैं। इनके अलावा
कलाम साहब वामपंथी, सामाजिक न्यायवादी
या क्षेत्रीय पार्टियों को देष के विकास में बाधा मानते हैं, जिनके
चलते कांगे्रस और भाजपा को गठबंधन सरकार चलाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। कलाम
साहब की जिस लोकप्रियता का विरुद गाया जाता है वह उसी जनता के बीच है जो विषाल
भारत के भीतर बनने वाले मिनी अमेरिका की निवासी है। मिनी अमेरिका के बाहर की जनता
पर उनकी लोकप्रियता लादी गई है।
नैयर साहब को मलाल है कि कलाम साहब के रहते
राष्ट्रपति पद के लिए किसी दूसरे उम्मीदवार के बारे में सोचा गया। अवकाष प्राप्त
करने की बेला में उन्होंने कलाम साहब से मुलाकात की और उनसे कोई खास खबर निकालने
की कोषिष की। लेकिन कलाम साहब का कमाल कि वे उनके ‘विजन
2020’,
जिसके तहत सन 2020 तक
भारत दुनिया का महानतम देष हो जाएगा, के
गंभीर रूप से कायल होकर बाहर निकले। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं और बहसों
पर गहरी पकड़ रखने वाले नैयर साहब ने ‘मिसाइल
मैन’
के समक्ष यह सवाल नहीं उठाया कि अगर सभी देष विकसित, महाषक्ति
और महानतम बनेंगे तो किसकी कीमत पर? भारत
2020 तक
विकसित महाषक्ति और महानतम हो जाएगा तो किस विचारधारा और रास्ते के तहत? नैयर
साहब की खुषी और बढ़ गई होगी जब कलाम साहब ने अपने विदाई भाषण में यह घोषणा की कि 2020 से
पहले भी भारत दुनिया का महानतम राष्ट्र बन सकता है। यह षीषे की तरह साफ है कि कलाम
साहब उसी राष्ट्र के विकास और महानता की बाात कर रहे हैं जिसे नवउदारवादी पिछले
डेढ़ दषक से बनाने में लगे हैं। कलाम साहब का आह्वान पूरी तरह से
अमरीकावादियों-नवसाम्राज्यवादियों की संगति में है। वरना कोई बताए कि एक अरब 20
करोड़ की आबादी का देष आधुनिक विज्ञान और तकनीकी, जिसके
कलाम साहब विषेषज्ञ हैं, पर आधारित पूंजीवादी
विकास के मॉडल के मुताबिक 2020 तक कैसे विकसित हो
सकता है?
क्या कहा जा सकता है कि अपने कार्यकाल में कलाम साहब ने
सपने नहीं, अंधविष्वास परोसे हैं!
सरकारी तंत्र और मीडिया में कलाम साहब की
गुणगाथा पूरे पांच साल सतत चलती रही। वह अगले पांच साल और चलती रहे इसके लिए कलाम
साहब के गुणगायकों ने एसएमएस के जरिए जोरदार प्रयास किया। लेकिन जब लगा कि
राष्ट्रपति का पद, जिसे उनकी नजर में
कलाम साहब ने अभूतपूर्व महानता और पवित्रता से मंडित कर दिया था, राजनीति
के गंदे कीचड़ में लथेड़ा जा रहा है, तो
गुणग्राहक दुखी हो गए। राजनीति कलाम साहब को बुरी लगती है तो उनके गुणगायकों को
कैसे अच्छी लग सकती है! गठन के समय से ही कलाम साहब के गुणगायक तीसरे मोर्चे का
उपहास उड़ाने और उन पर लानत भेजने में अग्रणी थे। लेकिन जैसे ही मोर्चे ने अपनी तरफ
से कलाम साहब का नाम चलाया, गुणगायक और खुद कलाम
साहब मोर्चे के मुरीद हो गए। काष कि मोर्चा उनकी जीत सुनिष्चित कर पाता और
गुणगायकों को कलाम साहब को आखिरी सलाम नहीं करना पड़ता! ‘कमाल
के कलाम साहब’ का आखिरी सलाम का कार्यक्रम एक ‘ग्रांड
फिनाले’
रहना ही था। हैरत यही है कि उसमें सबसे ऊंचा स्वर हमारे
आदरणीय सुरेंद्र मोहन जी और कुलदीप नैयर साहब का रहा।
कहना न होगा कि कलाम साहब के कमाल का मिथक
उनके गुणगायकों और मीडिया का रचा हुआ था। उनके पद से हटने के बाद अब वह कहीं नजर
नहीं आएगा। (ये गुणगायक और मीडिया अब किसी और बड़ी हस्ती को पकड़ेंगे जो उनके ‘मिषन
अमेरिका’
को वैधता प्रदान करे।) अंत की घोषणाओं के बावजूद इतिहास चल
रहा है। वहां ठोस विचार अथवा कार्य करने वाले लोगों की जगह बनती है। इसलिए इतिहास
में कलाम साहब की जगह गिनती भर के लिए होगी, जो
पदासीन हो जाने के नाते किसी की भी होती है। ऐसे में ज्ञान और अनुभव में पगे दो
वरिष्ठतम विद्वानों की कलाम साहब के बारे में इस कदर ऊंची धारणा का औचित्य किसी भी
दृष्टिकोण से समझ में नहीं आता। अगर अवकाष-प्राप्ति के अवसर की औपचारिकता मानें तो
वह वंदना के सुरों में एक सुर और मिलाने जितनी ही होनी चाहिए थी। लेकिन दोनों का
सुर भानुप्रताप मेहता सरीखों को भी पार कर गया, जिन्होंने
वंदना में व्याजनिंदा का भी थोड़ा अवसर निकाल लिया। (देखें, ‘इंडियन
एक्सप्रैस’ 25 जुलाई 2007
में प्रकाषित उनका लेख ‘प्राइम मिनिस्टर
कलाम?’)
धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में भी कलाम साहब
के राष्ट्रपतित्व पर कुछ चर्चा की जा सकती है। राष्ट्रपति के पद के लिए कलाम साहब
का नाम भले ही मुसलमानों को रिझाने के लिए समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम
सिंह ने चलाया हो, उनके नाम पर सहमति
बनने का वास्तविक कारण गुजरात में सांप्रदायिक फासीवादी नरेंद्र मोदी की सरकार
द्वारा हजारों मुसलमानों की हत्या और बरबादी था। अगर गुजरात में राज्य-प्रायोजित
हिंसा में मुसलमानों का नरसंहार न हुआ होता तो कलाम के नाम पर भाजपा तो तैयार नहीं
ही होती,
उस सांप्रदायिक हिंसा और उसके कर्ता को रोकने में खोटा
सिक्का साबित हुई कांग्रेस भी कदापि तैयार नहीं होती। यह कहने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन
वास्तविकता यही है कि कलाम साहब को राष्ट्रपति का पद एक मुसलमान होने के नाते
गुजरात में मुसलमानों की हत्याओं के बदले तोहफे में मिला था। अगर कोई संजीदा इंसान
होता तो वह विनम्रतापूर्वक उस ‘सांप्रदायिक’ आम
सहमति से इनकार कर देता और वैसा करके धर्मनिरपेक्षता के साथ ही मानवता की नींव भी
मजबूत करता। हमारी यह मान्यता अनुबोध (ंजिमत जीवनहीज) पर आधारित नहीं है। गुजरात
के कांड के बाद उनके नाम पर बनी सहमति के वक्त हमने अपनी भावना एक कविता लिख कर अभिव्यक्त की थी जो
‘सामयिक
वार्ता’
में प्रकाषित हुई थी। अपने लेख की षुरुआत में सुरेंद्र मोहन
जी ने भी इस वास्तविकता का जिक्र किया है : ‘जब
इस पद के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने उनका नाम प्रस्तावित किया
था,
तब उसे अपनी छवि सुधारने के लिए एक मुस्लिम नाम की जरूरत थी, क्योंकि
गुजरात के घटनाक्रम के कारण उसका चेहरा दागदार बन गया था। लेकिन इन पांच वर्षों
में किसी नागरिक को यह पहचान याद नहीं आई। वे ऐसी सांप्रदायिक, जातिगत
या क्षेत्रीय गणनाओं से कहीं ऊपर उठे हुए थे और पूरे देष में यह सहमति थी कि वे
उसी पद पर दोबारा आसीन हों।’ यह सही है कि कलाम
साहब सांप्रदायिक, जातिगत और क्षेत्रीय
गणनाओं से ऊपर रहे। यह बड़ी बात है और अभी तक देष के हर राष्ट्रपति ने इसका निर्वाह
किया है। लेकिन इससे यह वास्तविकता निरस्त नहीं होती कि कलाम साहब का चयन, जैसा
कि खुद श्री सुरेंद्र मोहन जी ने कहा है, सांप्रदायिक
आधार पर हुआ था। अगर वे सांप्रदायिक आधार पर होने वाले अपने चयन को नकार देते तो
उनका बड़प्पन हमारे जैसे लोग भी मानते और उन्हें बगैर राष्ट्रपति बने भी सलाम करते।’’
जाहिर है, राष्ट्रपति
चुनाव के संदर्भ में कलाम साहब का व्यवहार भी गरिमापूर्ण नहीं कहा जा सकता। वे
पिछली बार भी राष्ट्रपति बनना चाहते थे और इस बार भी ऐन चुुनाव के मौके पर सक्रिय
हो गए। सवाल सर्वानुमति का नहीं, जीत का था। अगर जीत
की संभावना होती तो वे कंटेस्ट भी कर सकते थे। पहले की तरह उन्हें इससे फर्क नहीं
पड़ता कि कौन-सी पार्टियां उनका समर्थन कर रही हैं। जैसे उनकी भारत के महाषक्ति होने
की धारणा पर अढ़ाई लाख किसानों की आत्महत्याओं से कोई फर्क नहीं पड़ता।
धर्मनिरपेक्षता के दावेदार :
कितने गाफिल कितने खबरदार
राष्ट्रपति के उम्मीदवारों की चर्चा में
भाजपा के भावी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार पर भी चर्चा चल निकली। आरएसएस ने नरेंद्र
मोदी का नाम आगे किया तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने को धर्मनिरपेक्षता
का बड़ा दावेदार सिद्ध करने के लिए आगे आ गए। क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव पर 2014
में होने वाले आम चुनाव की छाया है। लिहाजा, नीतीष-नरेंद्र
मोदी प्रकरण पर भी थोड़ी चचा्र वाजिब होगी।
‘गुड़ खाना परंतु गुलगुलों से परहेज करना’ - बिहार
के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर इस कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। 2004 के
पहले केंद्र में जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राजग की सरकार बनी थी तो
उसका समर्थन करने और उसमें शामिल होने वाले नीतीश कुमार जैसे नेताओं ने कहा था कि
भाजपा की तरफ से ‘उदार’ वाजपेयी
की जगह अगर ‘कट्टर’ अडवाणी
प्रधानमंत्री बनाए जाते तो वे राजग सरकार का न समर्थन करते, न
उसमें शामिल होते। धर्मनिरपेक्षता की दावेदारी जताते हुए अपनी इस शर्त का उन्होंने
काफी ढिंढोरा पीटा था। हालांकि कुछ समय बाद उसी सरकार में अडवाणी उपप्रधानमंत्री
बनाए गए और मंत्री बने नीतीश कुमार ने कोई आपत्ति नहीं उठाई थी। वे पूरे समय राजग
सरकार में मंत्री रहे और बिहार में भाजपा के साथ मिल कर बतौर मुख्यमंत्री दूसरी
बार सरकार चला रहे हैं। गुजरात कांड उनके लिए घटना से लेकर आज तक कोई मुद्दा नहीं
रहा। लेकिन बीच-बीच में नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत विरोध का शगल करते रहते हैं।
गोया नरेंद्र मोदी अपने संगठन से अलग कोई बला है!
राजनीतिक सफलता ने नीतीश कुमार को आश्वस्त
कर दिया है कि आरएसएस-भाजपा के साथ लंबे समय तक राजनीति करके भी वे धर्मनिरपेक्ष
बने रह सकते हैं। यह स्थिति नीतीश कुमार से ज्यादा धर्मनिरपेक्षता के अर्थ पर एक
गंभीर टिप्पणी है। मुख्यधारा राजनीति में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ भाजपा के साथ रह
कर या भाजपा का भय दिखा कर मुसलमानों के वोट हासिल कर लेना है। जाहिर है, धर्मनिरपेक्षता
का यह अर्थ संविधान में प्रस्थापित धर्मनिरपेक्षता के मूल्य के पूरी तरह विपरीत और
विरोध में है। भाजपा आरएसएस का राजनैतिक मंच होने के नाते स्वाभाविक रूप से
सांप्रदायिक है। भारतीय संविधान के तहत राजनीति करने की मजबूरी में उसे अपनी
सांप्रदायिकता को ही सच्ची धर्मनिरपेक्षता प्रचारित करना होता है। दूसरे शब्दों
में,
एक राजनीतिक दल के रूप में भाजपा संविधान के साथ धोखाधड़ी
करती है। लेकिन भाजपा के साथ या उसका भय दिखा कर मुस्लिम वोटों की राजनीति करने
वाले दल और नेता भी संविधान के साथ वही सलूक करते हैं।
कहने का आशय है कि पिछले 25
साल की राजनीति में धर्मनिरपेक्षता के मूल्य को जो लगातार ठोकरें खानी पड़ रही हैं, उसके
लिए अकेले सांप्रदायिक ताकतों को दोष नहीं दिया जा सकता। सांप्रदायिकता उनका ‘धर्म’ है।
इसमें धर्मनिरपेक्ष ताकतों का दोष ज्यादा है, क्योंकि
वे धर्मनिरपेक्षता की दावेदार बन कर उसका अवमूल्यन करती हैं। यह परिघटना राजनीति
से लेकर नागरिक समाज तक देखी जा सकती है। और असली खतरा यही है।
नरेंद्र मोदी का विरोध करने पर आरएसएस ने
भले ही नीतीश कुमार को धता बताई हो, लेकिन
नीतीश कुमार आरएसएस की बढ़ती का ही काम कर रहे हैं। आरएसएस शायद यह जानता भी है।
उसने सेकुलर नेताओं और बुद्धिजीवियों को अपने ‘आंतरिक
झगड़े’
में उलझा लिया है। वह नरेंद्र मोदी पर दांव लगा कर अडवाणी
के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ कर रहा है। जैसे अडवाणी के सामने वाजपेयी ‘उदार’ हुआ
करते थे,
वैसे अब नरेंद्र मोदी के मुकाबले अडवाणी उदार बन जाएंगे।
आगे चल कर जब ‘गुजरात का शेर’ अडवाणी
जैसा नखदंतहीन बूढ़ा हो जाएगा तो उसके प्रधानमंत्री बनने का रास्ता भी साफ होगा।
क्योंकि तब तक हिंदुत्व का कोई और नया शेर आरएसएस में पैदा हो चुका होगा। खुद मोदी
उस तरह के कई शेरों के साथ प्रतियोगता करके अव्वल आए हैं। जब मोदी को गुजरात का
मुख्यमंत्री बनाया गया था तो उनसे पहले उस समय कट्टरता के मामले में उनसे कहीं
ज्यादा प्रख्यात प्रवीण तोगड़िया का नाम था। मोदी ने उन्हें पछाड़ कर मुख्यमंत्री का
पद हासिल किया था। यह जानकारी अक्सर दोहराई जाती है कि मोदी की कट्टरता से वाकिफ ‘उदार’ वाजेपयी
ने आरएसएस-भाजपा को आगाह किया था। साथ ही यह कि गुजरात कांड के मौके पर वाजपेयी ने
मोदी को राजधर्म निभाने की नसीहत दी थी। लेकिन होने वही दिया जो हुआ। आरएसएस की ‘उदारता’ की
बस इतनी ही सिफत है।
आरएसएस यह जानता है कि मनमोहन सिंह के बाद
देश के पूंजीपतियों की पहली पसंद नरेंद्र मोदी हैं। खुद मनमोहन सिंह के वे चहेते
हैं। नरेंद्र मोदी को भी अपनी हिंदुत्ववादी हुंकार के साथ सबसे ज्यादा भरोसा
पूंजीपतियों का है। वे पूंजीपतियों के बल पर इठलाते हैं। पूंजी के पैरोकार इधर
लगातार कह रहे हैं कि गुजरात कांड अब को भुला देना चाहिए। उनका तर्क है इससे देश
के विकास में बाधा पैदा हो रही है। यानी मोदी ने गुजरात को विकास का मरकज बना दिया
है। अब उन्हें देश के विकास की बागडोर सौंप देनी चाहिए। विदेशी पूंजी को मुनाफे से
मतलब होता है। वह मुनाफा मनमोहन सिंह कराएं या मोदी, इससे
विदेशी पूंजी को सरोकार नहीं है। इसलिए हो सकता है मोदी को अडवाणी जैसा लंबा
इंतजार न करना पड़े। दरअसल, यह खुद नरेंद्र मोदी
के हक में है कि वे इस बार अडवाणी को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में आगे
रहने दें। वे रहने भी देंगे। फिलहाल वे जो फूं-फां वे कर रहे हैं, वह
भविष्य के कतिपय दूसरे दावेदारों को दूर रखने के लिए है।
आरएसएस के भीतर कट्टरता और उदारता का यह द्वंद्व
चलते रहना है। भारतीय समाज की बहुलताधर्मी बनावट के चलते आरएसएस के लिए अपने भीतर
इस तरह का द्वंद्व बनाए रखना जरूरी है। इससे गतिशीलता का भ्रम तो रहता ही है; ऊर्जा
भी मिलती है। अडवाणी नीत उग्र राममंदिर आंदोलन ने आरएसएस-भाजपा कार्यकर्ताओं में
अपूर्व ऊर्जा का संचार किया। मस्जिद टूटी, दंगे
हुए,
मुस्लिम अलगाववाद बढ़ा और अंत में ‘उदार’ वाजपेयी
प्रधानमंत्री बने। मस्जिद ध्वंस के 10
साल बाद हुए गुजरात कांड ने भी आरएसएस-भाजपा कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार
किया। उस ऊर्जा का रूप भयानक था। उसकी फसल ‘उदार’ अडवाणी
काट सकते हैं। हिंदू धर्म का बाजार में जो तमाशा बन रहा है, उसके
चलते कभी ऐसा हो सकता है कि हिंदू धर्म की वास्तवकि उदार धारा आरएसएस की छद्म
उदारता से भ्रमित (कन्फ्यूज) हो जाए। आरएसएस की वह बड़ी जीत होगी।
आरएसएस जितनी आरामदायक स्थिति में आज है, वैसा
कभी नहीं रहा। समाज में उसकी व्यापक स्वीकृति और प्रभाव है जो निरंतर बढ़ता जा रहा
है। राजनीति में तथाकथित सेकुलर पार्टियां और नेता तथा गैर-राजनीतिक सिविल सोसायटी
आंदोलन उसमें मदद कर रहे हैं। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के दोनों सितारे - अन्ना
हजारे और रामदेव - नरेंद्र मोदी और आरएसएस के प्रशंसक ही नहीं हैं; यह
पूरा आंदोलन फासीवादी-तानाशाही रुझान लिए है। (आंदोलन के इस तरह के चरित्र का
विस्तृत विश्लेषण हमने ‘युवा संवाद’ में
लिखे कई लेखों में किया है।) आरएसएस के लिए इससे ज्यादा मुफीद क्या होगा कि अनेक
छोटी-बड़ी सेकुलर हस्तियां इस आंदोलन की कहार बनी हुई हैं। धर्म का राजनैतिक
इस्तेमाल सांप्रदायिकता का मुख्य किंतु अपूर्ण अर्थ है। धर्म को बाजार के भाव
बेचना और समाज को अंधविश्वासों में झोंकना भी सांप्रदायिकता में शामिल है। इस
भरे-पूरे अर्थ में सांप्रदायिकता का कारोबार जितना भरपूर आज चल रहा है, भारत
में पहले कभी नहीं चला।
इसे थोड़ा और पीछे जाकर देखें। देश की सबसे
बड़ी पार्टी कांग्रेस सांप्रदायिक कार्ड खेलती है तो वह भी आरएसएस का ही काम करती
है। कांग्रेस ऐसा एक बार नहीं, अनेक बार करती है।
समाजवादी पार्टी से बाहर आने पर बेनीप्रसाद वर्मा ने बताया था कि जब बाबरी मस्जिद
का ध्वंस हो रहा था तो उन्होंने मुलायम सिंह को कहा था कि समाजवादी पार्टी को आगे
बढ़ कर इसका विरोध करना चाहिए। लेकिन, बेनीप्रसाद
वर्मा के मुताबिक, मुलायम सिंह ने यह
कहते हुए हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया कि मस्जिद ध्वंस से उनकी पार्टी की ताकत
मजबूत होगी। बाद में मस्जिद ध्वंस के नायक कल्याण सिंह के साथ उन्होंने सरकार बनाई
और भाजपा-आरएसएस का बखूबी सहारा लिया। फरवरी 2002
में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुसलमानों के राज्य प्रायोजित खुले नरसंहार पर
कुछ कट्टर आरएसएस वालों ने भी दांतों तले उंगलियां दबा ली थीं। लेकिन उसके बाद
होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव में मायावती नरेंद्र मोदी का चुनाव प्रचार करने
गुजरात गई थीं। उन्होंने मोदी के साथ एक मंच से उन्हें जिताने की अपील की थी।
क्योंकि यूपी में उन्हें भाजपा के साथ सरकार बनानी थी।
लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास
पासवान वाजपेयी सरकार में मंत्री थे। भारत की राजनीति में झूठ बोलना बुरा नहीं, कला
माना जाता है। पासवान गुजरात कांड के बाद बाकायदा राजग सरकार में बने रहे।
उन्होंने दलित राजनीति में अपनी प्रतिद्वंद्वी मायावती को यूपी में समर्थन न देने
के लिए भाजपा पर दबाव डाला। भाजपा के उनकी बात न स्वीकार करने पर उन्होंने वाजपेयी
सरकार से इस्तीफा दिया। जबकि वे पाकिस्तान तक कह आए हैं कि उन्होंने गुजरात कांड
के विरोध में इस्तीफा दिया था। उड़ीसा में ग्राहम स्टेंस और उनके बच्चों को जिंदा
जलाने पर जॉर्ज फर्नांडीज ने संसद में आरएसएस का बचाव किया था। राजग सरकार में
शामिल रहे तेलुगु देशम के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू को भी सांप्रदायिक भाजपा से कोई
आपत्ति नहीं रही है। तृणमूल कांग्रेस, बीजू
जनता दल,
अन्ना द्रमुक, द्रमुक, जनता
दल (सेकुलर) असम गण परिषद, लोकदल, नेशनल
कांफ्रेंस आदि धर्मनिरपेक्ष माने जाने वाले दल और उनके नेता बिना झिझक
आरएसएस-भाजपा के सहयोगी बनते हैं।
जीवन की तरह राजनीति में भी तात्कालिक के
साथ दूरगामी लक्ष्य निर्धारित होते हैं। आरएसएस और इन तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों
में फर्क यह है कि ये दल महज सरकार बनाने अथवा सत्ता में हिस्सेदारी करने के
तात्कालिक लक्ष्य से परिचालित होते हैं। जबकि आरएसएस के लिए सरकार बनाने, राजनीतिक
सत्ता पाने से ज्यादा समाज में अपनी विचारधारा फैलाना महत्वपूर्ण है। हाल के
भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में वह भाजपा की अगली सरकार बने, इससे
ज्यादा इसलिए शरीक है कि समाज में उसकी वैधता बढ़ रही है और विचारधारा भी।
भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के
बतौर नरेंद्र मोदी की जगह अडवाणी का नाम आएगा तो नीतीश कुमार उसे अपनी जीत
बताएंगे। लेकिन, जैसा कि ऊपर बताया गया है, वह
आरएसएस की जीत होगी। और भी, अडवाणी आएंगे तो
सिविल सोसायटी आंदोलन के कई सेकुलर नेता सरकार या उसे बनाने और चलाने के इंतजाम
में शामिल हो सकते हैं। यह तर्क देते हुए कि उन्होंने कट्टर नरेंद्र मोदी को आगे
नहीं आने दिया। नीतीश कुमार जैसे ‘धर्मनिरपेक्ष’ नेता
उनका स्वागत करने के लिए पहले से वहां मौजूद होंगे। उदाहरण के लिए, राजग
की सरकार बनने पर, अपने पिता का इतिहास
दोहराते हुए प्रशांत भूषण बहुत विनम्रतापूर्व कानून मंत्री बन सकते हैं। उस सरकार
अथवा इंतजाम में अडवाणी के विश्वासभाजन अरविंद केजरीवाल का भी ऊंचा मुकाम होगा।
रामदेव से राष्टीय स्वाभिमान का पाठ पढ़ने वाले पूर्व के कुछ जनांदोलनकारी और
विकल्पवादी भी उसमें कुछ न कुछ काम का पा जाएंगे। कहने की जरूरत नहीं, अन्ना
हजारे और रामदेव उस सरकार के नैतिक प्रतीक और प्रेरणास्रोत होंगे।
अभी तक के अनुभव से कह सकते हैं पिछले 25
सालों का नवउदारवाद सबसे ज्यादा आरएसएस को फला है। इन दोनों - नवउदारवाद और
संप्रदायवाद - ने मिल कर सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय संविधान का किया है। इस दौरान
संविधान के नीति- निर्देशक तत्व किसी भी राजनीतिक पार्टी और नेता के लिए प्रेरक
नहीं रहे हैं। देश के संसाधनों को उसकी मेहनतकश जनता के अधिकार से छीन कर
देशी-विदेशी मुनाफाखोर कंपनियों को मोटी रिश्वतें खा कर बेचा जा रहा है। शिक्षा से
लेकर सुरक्षा तक की व्यवस्था को पूंजीवादी सांचे में ढाला जा रहा है। आबादी के
अधिकांश हिस्से को नवउदारवादी नीतियों के उच्छिष्ट पर जिंदा रहने के लिए मजबूर कर
दिया गया है। यहां तक कि मौलिक अधिकारों पर गहरा संकट आ पड़ा है। बोलने की आजादी
छीन ली गई है। पूंजीवादी सत्ता के खिलाफ बोलने वालों पर देशद्रोह के मुकदमे दायर
किए जा रहे हैं और सजाएं सुनाई जा रही हैं। इसके खिलाफ न राष्ट्रपति चुनाव की बहस
में कोई पक्ष है, न दो साल बाद चुने
जाने वाले प्रधानमंत्री पर होने वाली बहस में। भारत की प्रगतिशील राजनीति
नवउदारवाद और उसकी घुट्टी पीकर और ज्यादा बलवान बने संप्रदायवाद के सामने झुक गई
है। नीतीश कुमार जैसे आत्मव्यामोह में गाफिल नेता शायद यह सच्चाई देख ही नहीं पा
रहे हैं। तभी उन्हें अपने टके के बोल सोने के लगते हैं - ‘गोल्डन
वर्ड्स कैन नॉट बी रिपीटिड!’
एक समय माना गया था कि जातिवादी राजनीति
सांप्रदायवादी राजनीति की काट करती है। उसे सामाजिक न्याय की राजनीति का अच्छा-सा
नाम भी दिया गया था। लेकिन अब स्पष्ट हो चुका है कि तथाकथित सामाजिक न्याय की
राजनीति सांप्रदायिक राजनीति की काट नहीं है। बल्कि उसे बढ़ाने का काम करती
है।
अंत में कह सकते हैं कि भारत की सरकारें
नवउदारवादी व्यवस्था को मजबूत करती जाएंगी, लेकिन
संविधान के अभिरक्षक राष्ट्रपति - वे प्रणव मुखर्जी हों, संगमा
साहब हों या डॉ. कलाम होते - उसके विरोध में परोक्ष टिप्पणी भी नहीं करेंगे। जो
कुछ लोग सच्चे संघर्ष में जुटे हैं वे अपने ज्ञापन महामहिम को पहले की तरह सौंपते
रहेंगे। केवल यह नहीं कि सरकारें उन पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगी, खुद
राष्ट्रपति को वे निरर्थक लगेंगे। राष्ट्रपति चुनाव के साथ सार्थकता का संघर्ष
कितना कठिन हो गया है?
26 जून
2012
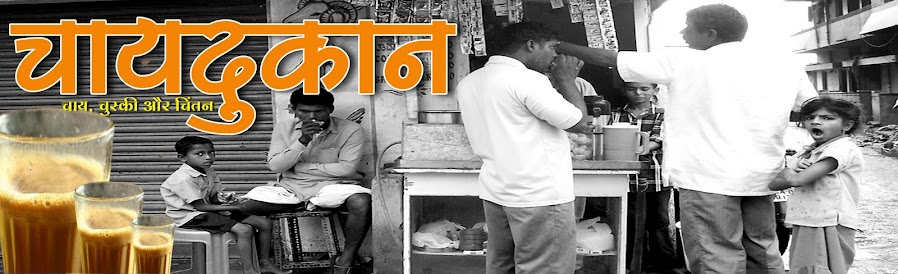
.jpg)